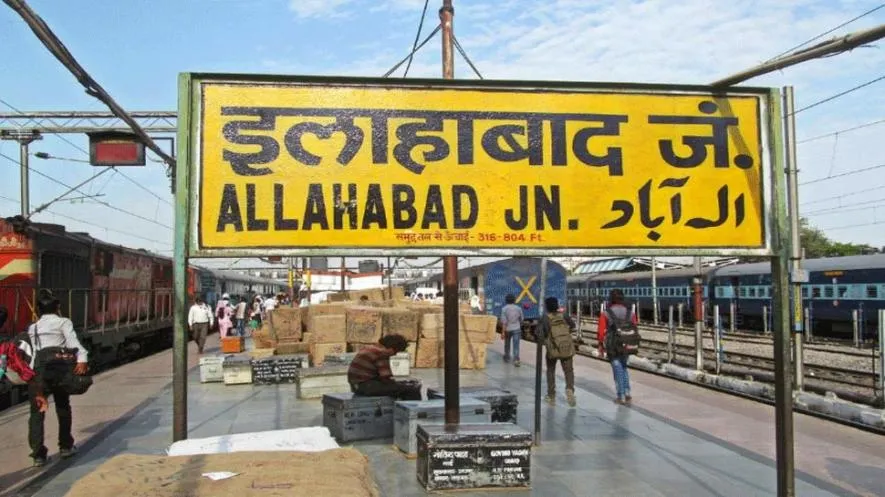सुबह के सात बजते ही उत्तर प्रदेश के महाराजगंज जिले का सोनौली कस्बा जाग उठता है। नेपाल की ओर जाने वाली पतली सड़क पर साइकिल, रिक्शा, ट्रैक्टर और पैदल यात्रियों की छोटी-छोटी कतारें दिखने लगती हैं। बिना पासपोर्ट, बिना वीजा लोग यूँ ही मज़े-मज़े से सरहद पार करते हैं, मानो यह कोई जिला मुख्यालय की सीमा हो। दोनों तरफ के पुलिस चौकियों पर हल्की-फुलकी पूछताछ जरूर होती है, पर औपचारिक कागज़ी जांच नहीं। यह नज़ारा बताता है कि भारत और नेपाल के बीच नेपाल बॉर्डर सिर्फ एक भूगोलिक रेखा है, दीवार नहीं।
1950 की इंडो-नेपाल संधि उस दौर के नेताओं की दूरदर्शी सोच
आज से पचहत्तर साल पहले, 31 जुलाई 1950 को दिल्ली के रोशनारो हाउस में भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और नेपाल के राजा त्रिभुवन के प्रतिनिधियों ने ‘भारत-नेपाल शांति और मित्रता संधि’ पर दस्तखत किए थे। ठीक उसी समय दुनिया की कई सीमाएँ कंटीली तार से घिर चुकी थीं, पर इन दोनों पड़ोसियों ने एक अलग रास्ता चुना। नेताओं ने तय किया कि लोग, माल और सेवाएँ बिना रोक-टोक गुजर सकें, ताकि इतिहास, संस्कृति और पारिवारिक रिश्तों की पुरानी डोर मजबूती से बंधी रहे। उस करार ने खुलेपन की जो बुनियाद रखी, वह आज भी कायम है।
खुली सीमा के प्रमुख प्रावधान और उनकी कानूनी बारीकियां
संधि के अनुच्छेद 6 और 7 नागरिकों को एक-दूसरे के देश में रहने, काम करने और संपत्ति खरीदने की सशर्त आज़ादी देते हैं। दोनों सरकारों ने यह भी माना कि सीमा पार लेन-देन पर कोई सीमा-शुल्क नहीं लगेगा, जब तक माल का कारोबार घरेलू उपयोग के लिए हो। हां, हथियार, मादक पदार्थ और जंगली जीवों की तस्करी को अपराध माना गया। दिलचस्प बात यह है कि आज तक इस समझौते को रद्द या संशोधित करने के लिए कोई औपचारिक नोटिस नहीं दिया गया। अदालतों में जब भी इसका ज़िक्र आता है, उसे एक जीवित दस्तावेज़ माना जाता है।
स्थानीय लोगों की जिंदगी में खुली सीमा का सीधा असर
महाराजगंज, कटिहार, जोगबनी, धौलपुर और काकरभिट्टा जैसे कस्बों में बसने वाले परिवारों के रिश्तेदार अक्सर सीमा के दोनों ओर फैले होते हैं। शादी-ब्याह, त्योहार या रोजमर्रा की खरीदारी—सब कुछ चंद मिनट की पैदल दूरी पर होता है। बचपन से लोग हिंदी, भोजपुरी और नेपाली का मिलाजुला ‘हिंदेपाली’ लहजा बोलते आ रहे हैं। भारतीय तरफ के बच्चों को नेपाल के इलाम से सस्ता चाय-पत्ती मिलती है, जबकि नेपाली किसान रक्सौल बाज़ार से ट्रैक्टर के पुर्ज़े लेने आते हैं। सीमा ने यहाँ रिश्ते कमज़ोर नहीं किए; उल्टा, रोजमर्रा के जीवन को आसान बनाया है।
रोज़गार, व्यापार और सांस्कृतिक आदान-प्रदान की अनकही कहानियां
दिल्ली में काम करने वाले कई नेपाली श्रमिक हर साल दशैं के समय घर लौटते हैं, तो दरभंगा के मिथिला कलाकार काठमांडू मेले में सिक्की घास की कलात्मक टोकरियाँ बेचते हैं। दोनों देशों के व्यापार का बड़ा हिस्सा अनौपचारिक है, पर इसका आर्थिक मूल्य अरबों रुपये आँका जाता है। खुले बॉर्डर ने छोटे कारोबारियों को वह लचीलापन दिया, जो बड़ी कंपनियों को बड़े कॉन्ट्रैक्ट से मिलता है। इसी खुली आवाजाही ने राम-जानकी यात्रा, बुद्ध पर्यटक सर्किट और कैलाश-मानसरोवर मार्ग जैसे सांस्कृतिक परियोजनाओं को भी व्यवहारिक बना दिया।
सुरक्षा चुनौतियां तस्करी से लेकर आतंकवाद तक की चिंताएं
खुली सीमा के फायदे जितने हैं, चुनौतियाँ भी उतनी ही गंभीर हैं। पिछले कुछ वर्षों में नकली करेंसी, मादक पदार्थ और हथियारों की तस्करी के मामले बढ़े हैं। सुरक्षा एजेंसियों का कहना है कि अपराधी भी इसी खुले रास्ते का फायदा उठाते हैं। 2015 के बाद से नेपाल में चीनी निवेश के बढ़ने पर कुछ भारतीय रणनीतिकारों ने खतरे की घंटी बजाई कि कहीं कोई बाहरी ताकत इस मार्ग का सैनिक उपयोग न कर ले। नतीजतन, संयुक्त गश्त, बायोमेट्रिक पहचान और संधि की समीक्षा जैसे सुझाव सामने आए हैं। फिर भी, दोनों सरकारें अब तक खुलेपन को बरकरार रखने पर सहमत हैं।
राजनीतिक बहसें और भविष्य के विकल्प
काठमांडू में कुछ राजनीतिक दलों का कहना है कि संधि असमान है, क्योंकि नेपाल पर सुरक्षा सम्बन्धी प्रतिबंध अधिक हैं। वहीं दिल्ली के कुछ विश्लेषक मानते हैं कि नेपाल की अर्थव्यवस्था भारत पर जरूरत से ज्यादा निर्भर है। संधि संशोधन की बात पहली बार 1996 में उठी थी, फिर 2016 में और अब एक बार फिर चर्चा तेज है। लेकिन हकीकत यह है कि सीमा बंद करना या वीज़ा लागू करना लाखों परिवारों को तुड़पाएगा। विशेषज्ञ मानते हैं कि समाधान सीमा को बंद करने में नहीं, बल्कि स्मार्ट प्रबंधन और पारदर्शी व्यापार प्रक्रियाओं में छिपा है।
साझा विरासत को संभालने की चुनौती और अवसर
भारत-नेपाल की खुली सीमा सिर्फ एशिया की नहीं, दुनिया की अनोखी मिसाल है, जहाँ दो स्वतंत्र देश बिना कंटीली तार के रह सकते हैं। 1950 की संधि ने भरोसे और सांझी विरासत की नींव डाली थी; आज वक्त की मांग है कि हम उसी भावना को आधुनिक व्यवस्थाओं के साथ जोड़ें। तकनीक, साझा सुरक्षा ढाँचा और युवाओं के लिए नए स्किल प्रोग्राम इस रिश्ते को और मजबूत कर सकते हैं। अगर दोनों सरकारें संवेदनशीलता के साथ काम करें, तो यह सीमा न सिर्फ आर्थिक फल देगी, बल्कि लोकतांत्रिक मूल्यों का भी जीता-जागता उदाहरण बनी रहेगी।