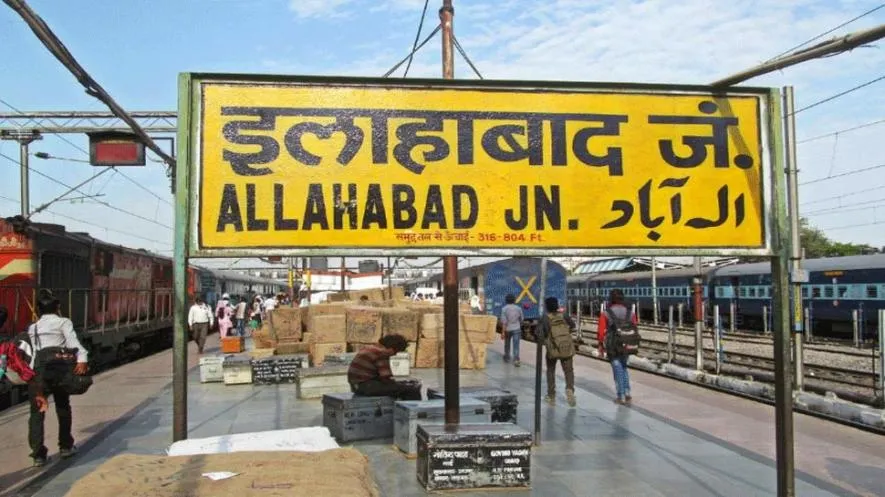रावी का बदलता रूप और बाढ़ से पैदा हुआ संकट पंजाब की रावी नदी सदियों से लोगों की ज़िंदगी से जुड़ी रही है। खेतों को पानी पहुंचाना हो या गांवों की रोज़मर्रा की जरूरतें — रावी का अपना अलग महत्व रहा है। इस बार बरसात आते ही नदी ने अचानक अपना रौद्र रूप दिखाया और दर्जनों गांव बाढ़ की चपेट में आ गए। घर, दुकानें, सड़कें और खेत पानी में डूब गए। कई परिवारों को रात भर में अपने घर छोड़कर सुरक्षित स्थानों की ओर भागना पड़ा।
इलाके के बुज़ुर्ग बताते हैं कि बरसात हर साल आती है और नदी उफान पर आती है, पर इस बार जो लहरें आईं, वे पहले कभी नहीं देखी गई थीं। लोगों के सवाल उठ रहे हैं — क्या केवल तेज बारिश ही इसकी वजह थी, या कहीं प्रशासनिक फैसला भी इस तबाही का कारण बना? जांच में जो बातें सामने आईं, वे यही संकेत देती हैं कि यह केवल प्राकृतिक घटना नहीं रही, बल्कि कुछ निर्णयन और उनकी टाइमिंग ने स्थिति और बिगाड़ दी।
बांधों से अचानक छोड़े गए पानी का असर और बड़ी गलती
जांच में साफ हुआ कि बाढ़ का सबसे बड़ा कारण बांधों से अचानक छोड़ा गया पानी रहा। जब जलस्तर बढ़ने लगा, तब सरकार या संचालन टीम ने बिना पर्याप्त तैयारी के एक साथ भारी मात्रा में पानी छोड़ा। इस पानी का बहाव निचले इलाकों पर पड़ने वाला दबाव बढ़ा गया और कुछ ही घंटों में कई गाँव पानी में डूब गए। ऐसे फैसले अचानक लिए गए, जिससे लोगों के पास बचने का समय नहीं बचा।
स्थानीय वकील और सामाजिक कार्यकर्ता कह रहे हैं कि अगर पानी नियंत्रित तरीके से धीरे-धीरे छोड़ा जाता और गांवों में समय से चेतावनी दी जाती तो नुकसान कम होता। अचानक छोड़े गए पानी ने कई घरों को उड़ोकर रख दिया — अनाज, कपड़े, घरेलू सामान सब पानी में बह गया। कुछ स्थानों पर लोग नावों से निकाले गए, कई लोग अस्थायी कैंपों में शरण लिए हुए हैं। इस तरह के निर्णयों की जवाबदेही और उनकी टाइमिंग पर अब गंभीर सवाल उठ रहे हैं।
ग्रामीण इलाकों की दुर्दशा और आम लोगों की परेशानी
बाढ़ का सबसे बड़ा असर किसानों और ग्रामीण परिवारों पर पड़ा। जहां पहले हरी-भरी फसलें थी, वहां अब पानी भरा खेत दिखते हैं। किसानों की आँखों की मेहनत और साल भर की कमाई कुछ ही घंटों में नष्ट हो गई। इससे उनकी आजीविका पर बड़ा झटका लगा है और आने वाले महीनों में खाद्य आपूर्ति और कीमतें भी प्रभावित हो सकती हैं।
घरों की हालत भी दयनीय है। कुछ मिट्टी के घर ढह गए, कुछ पक्के मकानों की दीवारें दरकी हुई हैं। बच्चों और बुज़ुर्गों के लिए हालात बहुत कठिन हैं — स्कूल बंद हैं, इलाज-इस्तेमाल मुश्किल है और साफ पानी की कमी बनी हुई है। राहत शिविर लगाए गए हैं, पर वहां भी भीड़ और संसाधनों की कमी लोगों की मुश्किलें बढ़ा रही है। कई परिवार खुले आसमान के नीचे रहने को मजबूर हैं और रोजमर्रा की जरूरतों के लिए जीवट संघर्ष कर रहे हैं।
पंजाब सरकार के फैसले और उठते सवाल
इस संकट ने सीधे तौर पर सरकार की नीतियों और फैसलों पर सवाल खड़ा कर दिया है। विपक्ष और स्थानीय लोगों का आरोप है कि प्रशासन ने समय पर चेतावनी नहीं दी और बांधों से पानी छोड़ने का निर्णय सही तरीके से नहीं संभाला। सरकार का जवाब यह रहा कि तेज बारिश और अचानक जलस्तर में वृद्धि के कारण परिस्थितियाँ कठिन हो गईं और टीमों ने नियंत्रण करने की कोशिश की।
फिर भी यह मुद्दा बार-बार उठता है कि क्या प्रशासन ने मौसम विभाग की चेतावनियों को गंभीरता से लिया था? क्या बांध संचालन के नियमों और मानकों का पालन हुआ? क्या गांवों में समय रहते अलर्ट जारी किए गए? ये ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब जनता मांग रही है। सिर्फ क्षतिपूर्ति की घोषणाएँ ही पर्याप्त नहीं होंगी; लोग चाहते हैं कि भविष्य में ऐसी लापरवाही दोबारा न हो।
जल प्रबंधन की खामियाँ और विशेषज्ञों की राय
विशेषज्ञ बताते हैं कि देश में जल प्रबंधन अभी भी पारंपरिक तरीकों पर निर्भर है। आधुनिक सेंसर, रीयल-टाइम मॉनिटरिंग और समय पर अलर्ट देने की व्यवस्था सीमित है। यदि बांधों पर आधुनिक उपकरण और सतत निगरानी होती तो पानी छोड़ने की योजना वैज्ञानिक आधार पर बनाई जा सकती थी और नुकसान घटता। मौसम के बदलते पैटर्न को देखते हुए पारंपरिक नियमों को अपडेट करने की जरूरत है।
जल विशेषज्ञों का सुझाव है कि बांध संचालन में पारदर्शिता होनी चाहिए और निर्णय लेने से पहले स्थानिय प्रशासन व नगर निकायों को सूचित किया जाए। स्थानीय लोगों को अलर्ट करने के लिए सायरन, मोबाइल संदेश और पंचायत स्तर पर पूर्व चेतावनी तंत्र मजबूत करना होगा। तकनीक, स्थानीय ज्ञान और प्रशासनिक प्रक्रिया का मेल ही भविष्य की बड़ी आपदाओं को रोक सकता है।
भविष्य के लिए सीख और जरूरी कदम
रावी की बाढ़ ने एक साफ संदेश दिया है — केवल प्रकृति को दोष देना पर्याप्त नहीं। हमें तैयारी, योजना और जवाबदेही के साथ आगे बढ़ना होगा। बांधों के रखरखाव, जल स्तर की सतत निगरानी और पानी छोड़ने के निर्णयों की वैज्ञानिक रूपरेखा बनानी चाहिए। गांवों तक समय पर चेतावनी पहुंचाने का तंत्र पहले से तैयार रखा जाए ताकि लोगों को सुरक्षित स्थल पर ले जाया जा सके।
राहत और पुनर्वास की योजनाएँ भी प्राथमिकता बननी चाहिए। केवल ऐन वक्त पर राहत दे देने से काम नहीं चलेगा; दीर्घकालिक पुनर्वास, मुआवजा और कृषि पुनर्स्थापना योजनाएँ लागू करनी होंगी। साथ ही जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को ध्यान में रखकर दीर्घकालिक नीतियाँ बनानी होंगी ताकि आने वाले वर्षों में ऐसी घटनाओं का प्रभाव कम किया जा सके।